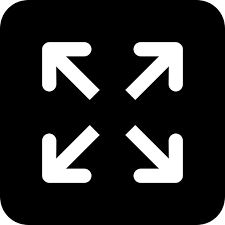मेधा और प्रतिस्पर्धा के बीच पीस रहे नौनिहाल
- डॉ. राकेश राणा
समाज की रुपरेखा, उसकी प्रकृति और प्रवृत्ति कैसी होगी यह भावी पीढ़ी पर ही निर्भर करता है। बच्चों का क्षमता निर्माण ही इस दिशा में किसी परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए बड़ा लक्ष्य होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट बताती है कि दुनियाभर में प्रति लाख पर औसतन 11.4 आदमी आत्महत्या कर रहे हैं। भारत में यह दर लगभग दोगुना है। यहां यह दर 20.9 प्रति लाख तक पहुंच गई है। भारतीय समाज में यह आंकड़ा इसलिए भी चिंता का विषय है कि अपने अध्ययन काल और जीवन के सबसे उत्पादक दौर में आत्महत्या का ग्राफ युवाओं में बढ़ा है। इनके पीछे विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक कारण तो हैं ही, हमारी मौजूदा शिक्षा प्रणाली भी इन आंकड़ों को बढ़ाने में भागीदार है। क्योंकि, भारतीय शिक्षा व्यवस्था सफलता से ज्यादा असफलताएं निर्मित कर रही है। शिक्षण संस्थानों में नामांकन का ग्राफ रॉकेट-रफ्तार पकड़े हुए है। परिणाम 'ढाक के तीन पात' की तरह बेरोजगारी के ग्राफ को समानान्तर संभाले हुए है।
समाज की सृजन शक्ति युवा-शक्ति दोहरे दबाव में जीने को अभिशप्त है। देश के महानगरों, नगरों और कस्बों में पौ फटने से पहले समाज के होनहार भावी कर्णधार हमारे बच्चे कत्लगाहों की तरह कोचिंगों में पहुंच जाते हैं, अपनी मेधा को तराशने और अपने भविष्य को तलाशने के नाम पर। वे अपने परिवार, समाज, राष्ट्र और देश-दुनिया के यथार्थ से कटकर अपनी तमाम शक्तियों, सृजनाओं और जूनून को प्रतिस्पर्धा को समर्पित कर देते हैं। यह वह शुरुआत है जो उन्हें धीरे-धीरे अनिश्चितताओं, तनाव, अवसाद और कभी-कभी तो आत्महत्या के आगोश तक ले जाती है। मेधा और प्रतिस्पर्धा के बीच बच्चे पीस रहे हैं। वे परीक्षाओं, प्रतियोगिताओं और प्रमाणिकताओं की अग्नि-परीक्षा देते-देते कुंठाओं और अविश्वासों से भरे भरभराकर गिर रहे हैं। क्योंकि, कैरियर बनाने की होड़ में परीक्षाओं की सफलताओं और असफलताओं की अपनी पारस्परिक सच्चाइयां हैं। सब अपने-अपने सत्यों के संघर्ष में जुटे दिखते हैं। युवाओं के सम्मुख सिविल सर्विसेज, मेडिकल, इंजीनियरिंग, प्रबंधन और सॉफ्टवेयर तथा मीडिया के कुछ क्षेत्र ही विकल्प हैं।
आकर्षक कैरियर का यह सीमित क्षेत्र प्रतिस्पर्धा से उपजे तनावों का अहम कारण है। हर कोई इन्हीं दायरों में अपने को आजमाने पर तुला है। देश की युवा-शक्ति का एक बड़ा हिस्सा इन्हीं प्रतियोगी परीक्षाओं में खुद को पीस रहा है। समाज की सृजनशील युवा ऊर्जा मेधा और प्रतिस्पर्धा की चक्की के दो पाटों के बीच चकरघिन्नी बना हुआ है। वह अपनी जीवन ऊर्जा का बड़ा हिस्सा अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते प्रतिस्पर्धा के सिन्ड्रोम में फांस देता है। प्रतियोगी परीक्षाएं एक फिल्टर की तरह काम कर रही हैं। परन्तु, फिल्टर की परम्परागत प्रवृत्ति के उलट। जो छनकर छानस हासिल हो रहा है वह सूक्ष्मांश मात्र है। वही सफलताओं में शुमार होता है और जो असफलताएं पैदा हुई, वे कई गुणा छनकर नीचे जमा हो रही बेरोजगारी का घेरा बड़ा करने का काम कर रही है। हर प्रतियोगिता में लाखों शिक्षित युवा आवेदन करते हैं जिनमें से मुट्ठीभर को चुनना होता है। इस पूरे नैराश्यपूर्ण परिदृश्य के बावजूद प्रतियोगी परीक्षाएं एक विचारधारा की तरह युवाओं के मानस को जकड़े हुए हैं। आंशिक लोगों की सफलताएं अधिकतम असफलताओं पर हावी हो जाती हैं। यही उस नैराश्यपूर्ण परिदृश्य को आशवस्त करता है कि पुनः जुटिये।
लोभ-मोह और अपेक्षाओं तथा पुनर्प्राप्तियों के लिए यह छद्म आशा निराशा को शहर के कर्फ्यू की तरह छांट डालती है। तनावपूर्ण स्थितियां नियंत्रण में नजर आने लगती हैं। तनाव के सामाजिक उपद्रव में तब्दील होने की संभावनाएं धीरे-धीरे समाप्त हो जाती है। यही प्रतियोगी परीक्षाओं के दर्शन की दक्षता है। निराशा से बड़ी आशा खड़ी करने के खेल में माहिर प्रतियोगी परीक्षाओं का बाजार ऐसा इन्द्रजाल बुने हुए है, जो बच्चों को, युवाओं को, उनके माता-पिताओं को और यहां तक कि नीति-निर्माताओं तक को लुभाने में सफल रहा है। परीक्षा मॉडल इतने प्रभावित करने वाले हैं कि नियमों, सिद्धांतों और पारदर्शिताओं से बुनी पृष्ठभूमि प्रतियोगियों और समाज में विश्वास पैदा करने में सफल और तार्किक दिखने लगती है। यही स्वीकार्यता असफलताओं पर समाज और सरकार की मुहर बैठवाने में कामयाब रहती है।
यही वह मनःस्थिति है जो प्रतिस्पर्धाओं की सत्ता और बाजार को बनाए हुए है। परिणामत: असफल लोग खुशी-खुशी अपनी असफलताओं की जिम्मेदारी अपने ऊपर डाल लेते हैं। पुनः और पुनः संघर्षों को जारी रखते हैं। प्रतिस्पर्धा का यह दर्शन ही आशा-निराशा के बीच सेतु निर्माण का काम करता है। नतीजतन, समाज की युवा पीढ़ी अपने सपनों और आकांक्षाओं को पाने की बजाय बाजार का झंडाबरदार बन जाती है। धीरे-धीरे थ्री-इडियट फिल्म की पटकथा के माकूल पात्र तैयार हो रहे होते हैं जो अपनी सृजनाओं-मौलिकताओं के हत्यारों की महत्वाकांक्षाओं और सपनों को पूरा करते-करते विक्षिप्त-सी मनोदशाओं में जीने को अभिशप्त हो जाते हैं। कैरियर प्रतिस्पर्धा का यह गढ़ा गया सामाजिक दर्शन पूरी व्यवस्था को पाक-साफ ढंग से बरी करा लेने में सफल रह जाता है। प्रतिस्पर्धा के मौजूदा दर्शन में स्थितियां, नियम-कानून और नीतियां सब शामिल हैं, तभी यह इतना टिकाऊ है। कोई नहीं पूछता कि जनसंख्या की बेतहाशा वृद्धि के बावजूद रोजगार सृजन के नये क्षेत्रों के विस्तार का क्या हुआ? प्रतिस्पर्धा-सिद्धांत की सीमाएं क्या हैं? इसकी वैधता क्या है?
बच्चों के मानवाधिकारों का क्या हाल है? युवाओं को किस प्रतिस्पर्धी-वैचारिकी की कंडीशनिंग से गुजरना पड़ रहा है? कोई सवाल नहीं ... हर तरफ सन्नाटा है। समाज, परिवार, सरकार सभी ने सहमति से मेधा और प्रतिस्पर्धा के दो पाटों वाली नदी में अपनी युवा ऊर्जा को फेंक रखा है। जहां धाराओं के विपरीत बहकर साबित करने की जद्दोजहद ही कैरियर निर्माण है। यह व्यवस्थाओं का आत्मघाती मॉडल है। ये किसी भी स्वस्थ समाज के संकेत नहीं हो सकते हैं। दुनिया के तमाम विकसित समाज धीरे-धीरे विक्षिप्त होने की दिशा में इन्हीं राहों पर बढ़ रहे हैं। क्या हमें व्यवस्थाओं से कड़ी पूछताछ नहीं करनी चाहिए कि मौजूदा विकास के मॉडल में रोजगार विस्तार की संभावनाएं कहां हैं? रोजगार के नये क्षेत्रों का विस्तार कहां है? योग्य युवाओं के लिए भी काम की कमी क्यों है? अवसरों की समानताएं क्यों नहीं है? ये तमाम मौजूं सवाल हैं। अस्तु, समाज और सरकार सबको मिलकर सोचना होगा कि हम अपने कोमल युवा-मस्तिष्कों के साथ कैसे न्याय करें?
(लेखक समाजशास्त्री हैं।)